भारत में लैंगिक असमानता (निबंध) Gender Inequality in India in Hindi
इस लेख में आप भारत में लैंगिक असमानता (निबंध) Gender Inequality in India in Hindi पढ़ेंगे। इसमें लैंगिक असमानता की परिभाषा, इतिहास, आँकड़े, प्रकार, कारण, प्रभाव, रोकने के उपायों के विषय में जानकारी दी गई है।
लैंगिक असमानता की परिभाषा Definition of Gender Inequality
असमानता एक बेहद बुरा शब्द है, जो हर तरफ से पक्षपात की तरफ इशारा करता है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य ऐसे पक्षपात अथवा असमानता से है, जो लिंग के आधार पर किया जाता है।
अधिकतर यह पक्षपात महिलाओं के साथ अधिक होता है। लैंगिक असमानता का अर्थ यह नहीं है कि हर तरफ केवल पुरुष अथवा केवल स्त्रियों की संख्या अधिक हो। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द है, जो लिंग के आधार पर भेद प्रकट करता है।
सबसे ज्यादा गति शील देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद भी समाज में आज तक लैंगिक असमानता का दानव जीवित है। यह बहुत पुराने समय से ही लोगों के बीच अपनी जगह बना चुका है।
लैंगिक असमानता महिलाओं के लिए बेहद दयनीय परिस्थिति होती है, जहां बचपन से लेकर अंत तक उनका शोषण, अपमान और भेदभाव किया जाता है। लैंगिक असमानता का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक विचारधारा को ठहराया जा सकता है।
भारत में लैंगिक असमानता का इतिहास History of Gender Inequality in India
इतिहास गवाह है कि जब भी लोग किसी रीति रिवाज का अर्थ अच्छे से नहीं समझने के बावजूद भी उसे अपना लेते हैं, तो वह कुप्रथा में परिवर्तित हो जाती है। लैंगिक असमानता आज व्यापक स्तर पर पहुंच गई है, यह सभी को पता है। लेकिन प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती जितनी कि आज है।
न जाने कितने ही तरह की प्रथाएं और रीति-रिवाजों ने महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है। किंतु प्राचीन समय में वैदिक काल में महिलाओं का वर्चस्व बहुत अधिक था।
बड़ी-बड़ी सभा और समितियों में भी महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व करती थी। यहां तक कि वेदों की रचना करने में योगदान देने वाली लोपामुद्रा तथा अपाला जैसी महान ऋषिकाएं भी उल्लेखित हैं। तो भला हमारा समाज इतना पक्षपाती कैसे बन गया जो पहले ऐसा नहीं था।
जिस तरह स्वेच्छा से किए गए दान को लोगों ने दहेज प्रथा में बदल दिया। इसी प्रकार न जाने कितने ही ऐसे महान रिवाज़ होंगे, जिन्हें लोग समझ नहीं पाए और उसे अंधश्रद्धा में तब्दील कर लिया।
महिलाओं के प्रति होने वाले अधिकतर पक्षपात इन्हीं अंधश्रद्धा और रीति-रिवाजों के कारण होता है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, और न जाने कितने ही अनगिनत प्रथाएं समाज में प्रचलित है।
भारत में लैंगिक असमानता के आँकड़े Gender Inequality in India Statistics 2020-2022
2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 146 देशों में से 135वां स्थान पर प्राप्त हुआ है। 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था।
2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में महिलाओं की संख्या में पुरुषों के मुकाबले सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारीक रिपोर्ट में भारत में लगभग 66 करोड़ से अधिक महिलाओं के आंकड़े दर्ज किए गए थे, जो कि अब 2021 से 22 में सुधार हुआ दिखाई दे रहा है।
लैंगिक असमानता के प्रकार Types of Gender Inequality in India)
घरेलू असमानता
भारतीय समाज में पुरुषों को अधिक वरीयता दी जाती है। उनकी अपेक्षा महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं होती है। कई बार यह असमानता माता-पिता और परिवार वालों की तरफ से किए जाते हैं।
पुत्रों को अधिक वरीयता देते हुए आज भी हमारे समाज में लोग कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हटते है। अक्सर स्त्रियों को वह करने की छूट नहीं होती है, जो भी वे करना चाहती हैं।
बुनियादी सुविधा में असमानता
यह पूरी तरह से एक अन्याय है, जहां बुनियादी सुविधाओं में भी लैंगिक असमानता किया जाता है। भारत सहित कई एशियाई व दूसरे महाद्वीप के देशों में शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिए कम अवसर मौजूद होते हैं। समाज ऐसा करने में बड़ा ही गर्व और सम्मान महसूस करता है।
स्वामित्व असमानता
स्वामित्व में भी महिलाओं और पुरुषों के बीच एक बड़ी असमानता देखी जाती है। पारिवारिक संपत्ति केवल पुरुषों का ही अधिकार बना रहता है। एक ही परिवार का होने के बावजूद भी माता पिता की संपत्ति पर एक स्त्री का कोई अधिकार नहीं रहता। यह समस्या भारतीय समाज में साफ देखी जा सकती है।
मृत्यु दर असमानता
भारत के कई राज्यों में महिलाओं और पुरुषों के लैंगिक अनुपात में बड़ा फर्क है। अक्सर लोग महिला शिशु की तुलना में पुरुष शिशु को वरीयता देते हैं।
जिसके कारण उनका बचपन से ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। यही कारण है महिलाओं की मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण युक्त आहार तथा अन्य ज़रूरी चीजें नहीं मिल पाता।
जन्मजात असमानता
लोगों की मानसिकता इतनी गिर गई है कि वह जन्मजात शिशुओं में भी भेद करते हैं। ऐसे ही दूषित मानसिकता वाले लोगों को यदि पता चले कि गर्भ में पल रहा शिशु एक महिला है, तो उसी समय कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध करने में यह लोग बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। भारत में टेक्नोलॉजी की सहायता से लिंग का चयन करके गर्भपात करना एक साधारण बात हो गई है।
विशेष अवसर असमानता
रूढ़िवादी और पुरानी सोच लिए हुए लोग अक्सर बच्चियों को वह अवसर नहीं प्रदान करते हैं, जो कि भविष्य निर्माण के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। उदाहरण स्वरूप शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण अवसरों में अक्सर लड़कियां पीछे रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे अवसर ही नहीं दिए जाते हैं।
रोजगार असमानता
अक्सर रोजगार के साधनों में भी महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं में पक्षपात किया जाता है। पुरुषों को उनके काम के लिए अधिक वेतन प्रदान किया जाता है, जबकि यदि उतना ही कार्य महिला करें तो लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते और वेतन भी कम प्रदान करते हैं। इसके अलावा पदोन्नति के मामले में भी लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है।
भारत में लैंगिक असमानता का कारण Causes of Gender Inequality in India
निरक्षरता
निरक्षर का तात्पर्य ऐसे लोगों से है, जिनके पास भले ही बड़ी-बड़ी शिक्षा की डिग्रियां मौजूद हों लेकिन उनकी विचारधारा वही घिसी पिटी होती है। समानता और मानवता की शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए।
गरीबी
गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, लैंगिक असमानता का। लोग बेटी पैदा होने पर इसे एक बहुत बड़ा कर्ज के रूप में देखते हैं। क्योंकि उन्हें उसके विवाह के लिए दहेज की चिंता सताने लगती है। ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा पुरुष शिशु को जन्म देने के पक्ष में रहते हैं।
पितृसत्तात्मक व्यवस्था
पुराने समय से चली आ रही पितृसत्तात्मक सोच की कड़ी अभी भी जारी है। यह व्यवस्था हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। जब तक इस पक्षपाती व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक लैंगिक असमानता को खत्म करना असंभव है।
महिलाओं में जागरूकता का अभाव
लैंगिक असमानता को कभी भी खत्म नहीं किया जा, सकता बसरते महिलाएं इसके लिए स्वयं जागरूक ना हो। आज भी करोड़ों महिलाएं लैंगिक असमानता का शिकार होती हैं क्योंकि वे अपने अधिकारों से वंचित है।
सामाजिक विश्वास
भारतीय समाज में बेटियों को बहुत नाजुक और दायित्व के रूप में देखा जाता है। वह लोग बेटों को अपने वृद्ध आयु में सहारा के रूप में देखते हैं। ऐसे लोगों को किरण बेदी, मैरी कॉम और दूसरी सफल महिलाओं के विषय में जरूर जानना चाहिए।
रोजगार का अभाव
ज्यादातर रोजगार के कामों में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। रोजगार के जितने साधन पुरुषों के लिए मौजूद हैं, उतने महिलाओं के लिए नहीं है। सीमित रोजगार के कारण भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलता है।
दुर्लभ राजनीतिक प्रतिनिधित्व
हमारे देश को आजादी मिले कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों के बाद देश पर शासन करने वाले लोग पितृसत्तात्मक है, यह कई मायने में कहना सही साबित होता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तो है लेकिन एक सीमित स्तर पर।
धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव
ऐसे हजारों साक्ष्य मौजूद है जो ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहते हैं कि जितने भी धार्मिक मान्यताएं हैं, अधिकतर वे महिलाओं पर लागू होते हैं।
जब धार्मिक नियम कानून एक महिला के मान सम्मान और महत्व पर आ जाए तो यह सरासर गलत हो जाता है। बहुत से ऐसे धार्मिक कानून है, जो महिलाओं के स्वतंत्रता को खोखला करते हैं।
पुरानी प्रथाएं
दुनियां कितनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी हम पुराने विचारों को ही लेकर बैठे हैं। जब तक समाज से पूरी तरह से कुप्रथा नष्ट नहीं होंगे, तब तक महिलाओं को उनका खोया हुआ सम्मान और अधिकार वापस नहीं मिल सकेगा।
भारत में लैंगिक असमानता का प्रभाव (effects of gender inequality in india)
सीमित रोजगार
गौरतलब है कि अधिकतर रोजगार पुरुषों के लिए ही उचित माने जाते हैं। यदि कोई महिला ऐसे किसी रोजगार में प्रतिनिधित्व करती है, तो फिर समाज के ताने भी सुनने पड़ते हैं। इस प्रकार सीमित रोजगार भी असमानता का एक कारण है।
दूषित मानसिकता का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास
एक उम्र के बाद यदि लोगों के धारणाओं में परिवर्तन नहीं आया, तो वह जीवन भर उसी विचार को लिए जीते रहेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी वही शिक्षा देंगे। इस तरह लैंगिक असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है।
आर्थिक निर्भरता
ना के बराबर स्वतंत्रता और सीमित रोजगार होने के कारण अधिकतर महिलाओं को अपने परिवार वालों पर अधिक निर्भर होना पड़ता है, जिसके कारण वे हमेशा दबाव महसूस करती हैं।
राजनिति में दुर्लब अवसर
राजनीति में महिलाओं की प्रधानता कई लोगों को रास नहीं आती है। बहुत ही मुश्किल से यदि कोई महिला राजनीति के बड़े पद पर पहुंच भी जाए, तो दूषित मानसिकता वाले लोग उनकी आलोचना करने से पीछे नहीं हटते हैं।
खेल जगत में कम महत्व
खेल की दुनिया में भी लैंगिक असमानता का प्रभाव साफ देखा जा सकता है, जहां किसी स्पर्धा में खेलने वाले पुरुषों को देखने वाली जनता के लिए भीड़ उमड़ती है। लेकिन वही महिला खिलाड़ियों के लिए ना के बराबर दर्शक आते हैं।
विज्ञान क्षेत्र में कठिन प्रवेश
कई लोगों को आज भी लगता है कि महिला पुरुषों के जितना कार्य और उन्नति नहीं कर सकती। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े ही मुश्किल से महिलाओं की भागीदारी होती है। यह लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है।
घरेलू हिंसा का शिकार
कई बार पारिवारिक झगड़े में महिलाओं को अपमान का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, जो विशेष तौर पर लैंगिक असमानता को दर्शाता है।
समाजिक समस्याएं
जब पूरा समाज ही दूषित मानसिकता लिए बैठा है, तो भला ऐसी कौन सी सुरक्षित जगह होगी जहां महिलाओं के साथ जादती न की जाए। यह बड़े दुख की बात है कि महिलाओं को केवल उनके कर्तव्य बताएं जाते हैं, लेकिन अधिकारों के विषय में कोई बात नहीं करना चाहता।
सीमित स्वतंत्रता
यह तो हर कोई जानता है कि किस तरह स्वतंत्रता के नाम पर भी महिलाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। चाहे परिवार हो या फिर पूरा समाज हर कोई महिलाओं को अपने मुट्ठी में रखना चाहता है।
मनोरंजन जगत में पक्षपात
मनोरंजन जगत भी लैंगिक असमानता से अछूता नहीं रहा है। कई अभिनेत्रियों और कलाकारों को भी इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है।
लैंगिक असमानता को भारत में कम करने के उपाय how to reduce gender inequality in india
महिला सशक्तिकरण
संगठन में शक्ति है। यदि महिलाएं सशक्त और स्वयं के अधिकारों के लिए जागरूक हो जाए, तो दुनिया में कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकेगा।
आर्थिक निर्भरता
दुनिया का सत्य है कि जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, तो लोगों का मुंह भी बंद हो जाता है। लैंगिक असमानता से लड़ने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है, कि महिलाओं को खुद आर्थिक निर्भर बनना पड़ेगा।
सरकारी योजनाएं
बीतते समय के साथ सरकार भी कई योजनाएं बेटियों के पक्ष में लाती रहती है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ‘ योजना जैसे कई थीम्स लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं और यह एक बहुत अच्छा कदम है।
परंपरागत धार्मिक विचारधारा
लोगों को अपने पुराने परंपरागत चले आ रहे विचारधारा में बदलाव करने की जरूरत है। तभी समाज में लोगों की सोच महिलाओं के विषय में बदलेंगे।
बच्चियों के जन्म पर आर्थिक सहायता
गरीब और मध्यम वर्ग में बेटी पैदा होने पर सरकार और दूसरी बड़ी संस्थाओं को जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। इससे लोगों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा मिलेगा।
बड़े पदों पर नियुक्ति
राजनीति हो या फिर कोई बड़ी कंपनी महिलाओं को उनका अधिकार पुनः दिलवाने के लिए लोगों को खुद आगे आना होगा और बड़े पदों पर उनकी क्षमता को परख कर न्याय करते हुए महिलाओं की भी नियुक्ति करनी चाहिए।
कानूनी व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन
भारतीय संविधान में ऐसे कई प्रावधान और नियम कानून है, जिन्हें लोग वास्तविकता में नहीं मानते हैं। लोग अपनी आदत से मजबूर है, यदि इस कानून व्यवस्था को सख्त कर दिया जाए और लोगों को इसका पालन करने के लिए बाध्य किया जाए, तो अवश्य असमानता को समानता में बदला जा सकता है।
शिक्षा पर बल
अगर किसी बेटी को अच्छी शिक्षा प्रदान किया जाता है, तो इससे एक पूरा परिवार शिक्षित बनता है, जिससे समाज में भी साक्षरता आती है। असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
लैंगिक समानता की जागरूकता
अंधविश्वास की तरह कृतियों का पालन करते आए लोगों को जागरूक बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। जिससे कि उन्हें लैंगिक समानता का असली इतिहास और इसका महत्व पता चल सके।
अपराध करने की सख्त सजा
कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और गर्भ में लिंग की जांच करने वाले लोग भी एक जीते जाते मनुष्य की हत्या करने वाले अपराधी के बराबर होते हैं। कानूनी अवस्थाएं तो बहुत सारी बनाए गए हैं, लेकिन जरूरत है उन्हें कड़ाई से पालन करने की जिससे लैंगिक समानता को बल मिल सके।
निष्कर्ष Conclusion
इस लेख में आपने भारत में लैंगिक असमानता (Gender Inequality in India in Hindi) के विषय में पढ़ा। आशा है यह लेख आपको जानकारी से भरपूर लगा होगा। अगर यह लेख आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें।
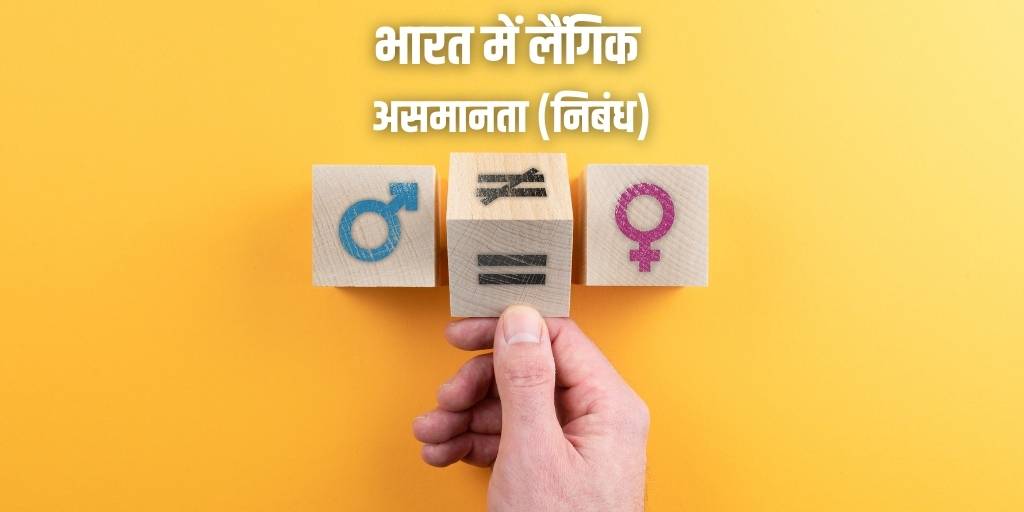
Very nice